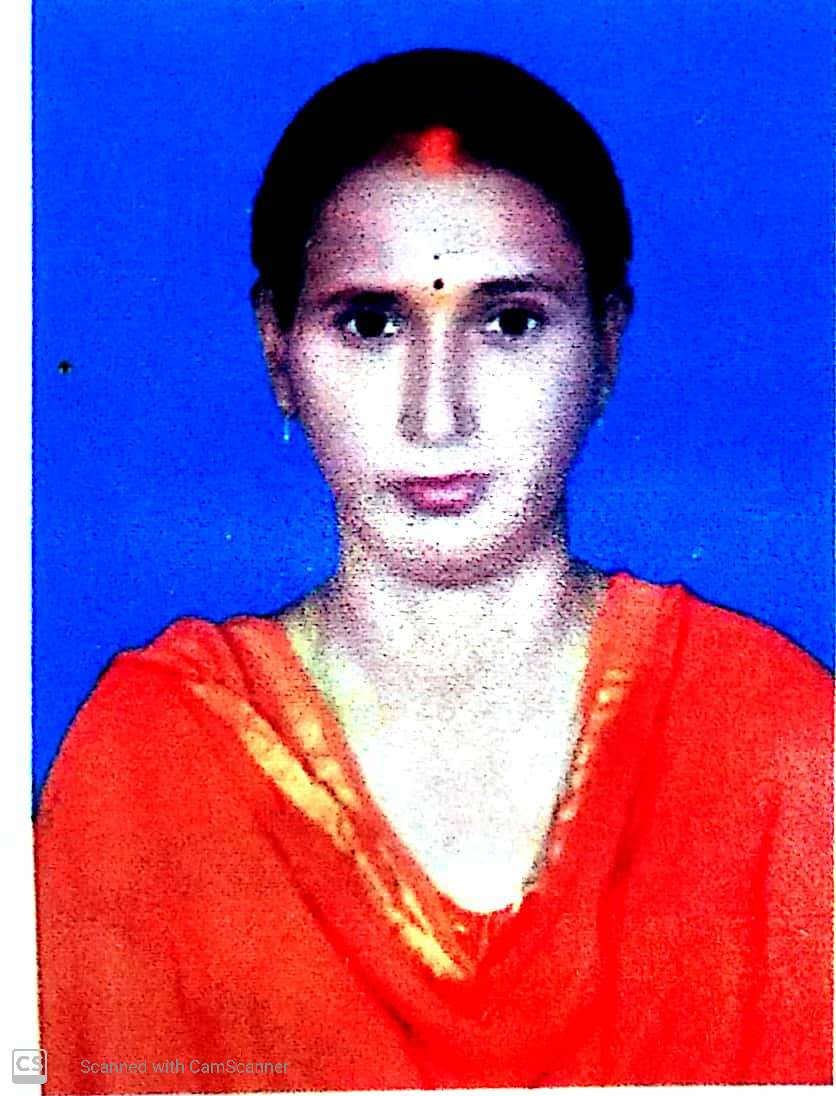|
|||||||
|
स्वतंत्रता के पश्चात् जय प्रकाश नारायण का सम्पूर्ण क्रांति में योगदान |
|||||||
| Contribution Of Jai Prakash Narayan In Total Revolution After Independence | |||||||
| Paper Id :
19770 Submission Date :
2025-02-12 Acceptance Date :
2025-02-21 Publication Date :
2025-02-25
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. DOI:10.5281/zenodo.14884167 For verification of this paper, please visit on
http://www.socialresearchfoundation.com/anthology.php#8
|
|||||||
| |||||||
| सारांश |
सम्पूर्ण क्रांति की शुरूआत जयप्रकाश नारायण ने की। जिसका मुख्य उद्देश्य पिछड़े जाति के पुरूष एवं महिला वर्ग को ऊंचता के शिखर पर पहुंचाना। इसके तहत् उन्होंने भ्रष्टाचार मिटाने, बेरोजगारी दूर करने शिक्षा में क्रांति लाने का प्रयास किया। 1975 ई. में जब इंदिरा गांधी पर चुनावों में भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जो साबित भी हो गया था। तब जयप्रकाश नारायण को इंदिरा गांधी ने जेल में डाल दिया था, 1977 ई. में जब आपात काल हटाया गया। तब उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया था। वे जनता के सेवक थे अतः उन्हें जनता ‘लोक नायक‘ के नाम से पुकारते थे। |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सारांश का अंग्रेज़ी अनुवाद | Jaiprakash Narayan started the Sampoorna Kranti. Its main objective was to take the men and women of backward castes to the pinnacle of heights. Under this, he tried to eradicate corruption, remove unemployment and bring revolution in education. In 1975, when Indira Gandhi was accused of corruption in elections, which was also proved. Then Jaiprakash Narayan was put in jail by Indira Gandhi. In 1977, when the emergency was lifted, he was released from jail. He was a servant of the people, so the people called him 'Lok Nayak'. |
||||||
| मुख्य शब्द | सांस्कृतिक, बौद्धिक, अध्यात्मिक, लोकनायक, सम्पूर्ण क्रांति, भारत रत्न, विधान सभा, भ्रष्टाचार, जन-संगठन, सदाचार। | ||||||
| मुख्य शब्द का अंग्रेज़ी अनुवाद | Cultural, Intellectual, Spiritual, People's Leader, Total Revolution, Bharat Ratna, Legislative Assembly, Corruption, Public Organization, Morality. | ||||||
| प्रस्तावना | जय प्रकाश नारायण देश की आजादी के पश्चात् देश में फैली अव्यवस्था को ठीक करने का प्रयास किया। इस दौरान उन्होंने इंदिरा गांधी को पद्च्यूत करने के लिए ‘‘सम्पूर्ण क्रांति‘‘ नामक आंदोलन चलाया। लोग उन्हें लोकनायक के नाम से विभूषित करते थे। 1999 ई. में उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। सम्पूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण का विचार था। जिसका आह्वान उन्होंने इंदिरा गांधी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए किया था। लोकनायक ने कहा कि इसके माध्यम से वे उन सभी मुद्दों पर लोगों का ध्यान आकर्षित करेंगे, जिसकी समाज को सबसे ज्यादा जरूरत है, जिनमें प्रमुख रूप से राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक व आध्यात्मिक। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में उन्होंने सम्पूर्ण क्रांति का आह्वान किया। मैदान में आए सभी लोगों ने जात-पात की भेद-भाव को मिटाकर समाज में प्रचलित बुराईयों को जड़ से मिटाने की कसम खाई थी, उसी मैदान में हजारों लोगों ने अपने जनेऊ तोड़ दिए थे। उस समय एक ही नारा गुंज था। ‘‘जात-पात तोड़ दो तिलक दहेज छोड़ दो। समाज के प्रवाह को नई दिशा में मोड़ दो।‘‘ जयप्रकाश नारायण ने युवाओं को आंदोलित कर दिया था। इसकी चिंगारी तो बिहार में उठी थी, लेकिन इसकी लौ पूरे भारत में फैल गई थी। इस समय वर्तमान के समय के कुछ नेता इस आंदोलन का हिस्सा थे। यथा लालू यादव, नीतिश कुमार, रामविलास पासवान, सुशील कुमार यादव। जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि ‘‘सम्पूर्ण क्रांति से मेरा तात्पर्य समाज के सबसे अधिक दबे-कुचले व्यक्ति को सत्ता के शिखर पर देखना है।‘‘ उन्होंने कहा कि इस क्रांति के माध्यम से समाज में प्रचलित सम्पूर्ण अव्यवस्था को व्यवस्थित कर देंगे। तब कहीं बदलाव हो सकेगा। इससे मनुष्य सुख-शांति का मुक्त जीवन जी सकेगा। इस दौरान उन्होंने एक वर्ष तक विश्वविद्यालय और कॉलेज को बंद करने का आह्वान किया। |
||||||
| अध्ययन का उद्देश्य | प्रस्तुत शोधपत्र जयप्रकाश नारायण द्वारा संचालित सम्पूर्ण क्रांति के परिपेक्ष्य में है, जिसमें उन सभी तथ्यों पर चर्चा की जायेगी जो इस शोधपत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। |
||||||
| साहित्यावलोकन |
प्रस्तुत शोध-पत्र विभिन्न पुस्तकों का अवलोकन करके तैयार किया गया है जिसका विश्लेषण शोधपत्र में किया गया है।
|
||||||
| सामग्री और क्रियाविधि | इस शोध में मुख्यतः ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक, वर्णात्मक विधि द्वारा कार्य सम्पन्न किया जायेगा। साथ ही साथ प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोत पर ध्यान केन्द्रीत किया जायेगा। |
||||||
| विश्लेषण | सम्पूर्ण क्रांति इस शब्द से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि, इसमें उन सभी तथ्यों पर ध्यान केन्द्रीत किया गया था। जिससे सम्पूर्ण समाज में बदलाव लाया जा सके। इससे समाज में प्रचलित कुरूतियों को दूर किया जा सकेगा। इस क्रांति के माध्यम से जयप्रकाश नारायण ने लोगों के मन में यह बात बैठी दी कि आप सभी का उत्थान तभी संभव है जब आप अपनी शक्ति पहचान पाऐंगे। इसके लिए समाज में प्रचलित सभी कुरूतियों से दूर होना होगा जो समाज के मार्ग के अवरोधक है। इसके लिए उन्होंने युवकों का ध्यान उन तथ्यों की ओर खिंचा, जिस पर चलकर वे अपने गांव, प्रदेश, देश का कल्याण कर सकेंगे। वे मुख्य तथ्य इस प्रकार से थे।
राजनैतिक इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान जिस प्रकार की राजनैतिक अव्यवस्था फैली हुई थी, उसे वह क्रांति के माध्यम से ठीक करने का प्रयास कर रहे थे। 5 जून 1974 ई. को विधान सभा में जयप्रकाश नारायण ने पहली बार सम्पूर्ण क्रांति का उच्चारण किया। इसके पश्चात् गांधी मैदान में जहां लाखों की भीड़ मौजूद थी, वहां लोगों के बीच अपने विचार प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि देश की गिरती हालत, प्रशासनिक, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, अनुपयोगी शिक्षा पद्धति एवं प्रधानमंत्री द्वारा अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का सुविस्तार उत्तर देते हुए जयप्रकाश नारायण ने सम्पूर्ण क्रांति के लिए जनता का आह्वान किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि यह क्रांति है मित्रों एवं सम्पूर्ण क्रांति है, विधान सभा का विघटन मात्र उद्देश्य नहीं है, यह तो महज मील का पत्थर है, हमारी मंजिल तो बहुत दूर है।[1] वे राजनीति में फैली अव्यवस्था को दूर करके समाज को व्यवस्थित करना चाहते थे। उनका कहना था कि अव्यवस्था सभी क्षेत्र में व्याप्त है, अतः सुधार भी सभी क्षेत्र का होना चाहिए। उन्होंने 7 जून को विधान सभा भंग करो अभियान चलाने तथा मंत्रियों और विधायकों को विधान सभा में प्रवेश से रोकने के लिए सभा के फाटकों पर धरना देने तथा प्रखण्ड में सचिवालय स्तर तक प्रशासन ठप्प करने, लोकशक्ति को बढ़ाने हेतु छात्र युवक एवं जन-संगठन बनाने, नैतिक मूल्य की सदाचारण करने एवं गरीब-कमजोर वर्ग की समस्याओं से निपटने के लिए भी छात्रों तथा जन साधारण को सम्पूर्ण क्रांति का हिस्सा बनने के लिए लोगों का आह्वान किए थे।[2] इसके पश्चात् जब सभा स्थल पर गोलियां चलाई गई। जिसमें 12 लोग घायल हो गए। तब सभा के लोगों की उत्तेजना तेज हो गई थी। पटना के जिलाधीश विजयशंकर दुबे के मतानुसार उस मकान में ‘‘इंदिरा बिग्रेड‘‘ नामक संगठन के कार्यकर्ता रहते थे, उनमें छः व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे। जिनमें से एक के पास से धुंआ निकलती बंदुक और छः गोलियां बरामद की गई थी। स्वयं अगर वहां जयप्रकाश नारायण नहीं मौजूद होते तो शायद उस शाम इंदिरा बिग्रेड के दफ्तर से लेकर विधान भवन सचिवालय आदि सबकुछ जल गया होता। प्रख्यात चिंतक आचार्य राममूर्ति के अनुसार 5 जून के विशाल प्रदर्शन को देखकर ऐसा महसूस हुआ कि पूरा बिहार खड़ा हो गया। सारे संघर्ष ने ‘‘सत्ता बनाम जनता‘‘ का रूप ले लिया था।[3] यह एक विशेष समय था जब बूढ़े एवं बीमार जे. पी. के हस्ताक्षरों के बण्डल ट्रक पर लाद कर राज्यपाल के घर ले जाए गए। जिसमें उल्लेखित था कि प्रचलित सत्ता में जनता का विश्वास नहीं रहा तथा इस बात की परोक्ष घोषणा थी कि उसे विश्वास है जे. पी. और उनके आंदोलन पर। लोगों ने जयप्रकाश नारायण का साथ देते हुए कहा कि हमें सम्पूर्ण क्रांति चाहिए इससे कम नहीं। इस अंादोलन का कार्यक्रम निम्न प्रकार से था।
विधान सभा के 24 सदस्यीय जनसंघ गुट के विधायकों में लालमुनी चौबे ने सर्वप्रथम इस्तिफा दिया। उनके साथ 12 विधायकों ने विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दिया। लेकिन आठ विधायकों ने पार्टी के निर्देश को ठुकरा दिया। जनसंघ ने इन आठ विधायकों को तथा तीन अन्य को पार्टी से छः वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया। शेष एक विधायक ने उसी वक्त त्याग पत्र दे दिया, इसके अलावे तेरह संसदीय संयुक्त सोशलिस्ट के 7 विधायकों ने इस्तिफा दे दिया। जबकि अन्य कुछ नेताओं ने इस्तिफा नहीं दिया। इस्तिफा देने वाले विधायकों ने यह मांग रखा कि 15 एवं 16 जून को कलकत्ता में हो रहे कांगेस संगठन ‘महासमिति‘ की बैठक को स्थगित किया जाए। इसके पश्चात् विधान सभा सामने 23 सत्याग्रही को गिरफ्तार किया गया। इसी दिन बिहार छात्र संघर्ष समिति ने छात्रों का आह्वाहन किया और कहा कि वे एक वर्ष तक अपनी कक्षाओं का बहिष्कार करें। इसके साथ ही वे सभी जयप्रकाश नारायण द्वारा संचालित सम्पूर्ण क्रांति का हिस्सा बनें। 25 जून 1975 ई. से 21 मार्च 1977 तक देश में आपातकाल लागू रहा। इस दौरान चुनाव स्थगित कर दिए गए। नागरिक अधिकारों को समाप्त कर मनमानी की गई। इंदिरा गांधी के राजनैतिक विरोधियों को कैद कर लिया गया। प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया। इसी दौरान जय प्रकाश नारायण को भी जेल में डाला गया। इस समय को ‘‘काली अवधि‘‘ कहा गया।[4] आर्थिक जनता को आर्थिक स्वतंत्रता दिलाने हेतु एवं उसे शोषण अन्याय, दरिद्रता से बचाने के लिए तथा उसे अज्ञानता से बाहर निकालने के लिए प्रमुख उद्योगों का राष्ट्रीयकरण के अतिरिक्त स्वराज-शासन को और किस प्रकार बेहतर बनाया जा सकता है, इस पर ध्यान केन्द्रीत किया। इस मंजिल को प्राप्त करने के लिए जो भी आवश्यक कदम थे, वे अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी दल ने तय किए। जो निम्न प्रकार से थे।
उत्पादक जनता को सारी सत्ता का हस्तांतरण उत्पादक जनता अर्थात वस्तुओं के उत्पादन में संकलन मजदूरों के हाथ या मस्तिष्क से सेवा करने वाली जनता की सारी सत्ता का राजनीतिक एवं आर्थिक सत्ता हस्तांतरण किया जाना समुची योजना की आधारशिला है, अगर सारी सत्ता श्रम करने वालों के हाथों में आ जाती है तब श्रम नहीं करने वालों के पास कोई सत्ता नहीं रहेगी। आरंभ से ही सत्ता श्रम करने वालों के पास न रहकर सम्पत्ति रखने वालों के पास रही है। यह आधुनिक लोकतंत्र से पहले एवं बाद की घटना से साबित हो जाता है। मतपेटिका तथा दलिय शासन पद्धति के उदय के साथ लोकतंत्र का आरंभ माना जाता है। जिससे उच्चतम् एवं निम्नतम वर्ग के हाथों में सत्ता का बंटवारा हो गया है लेकिन आर्थिक व्यवस्था का अधिकार सम्पत्ति वालों के पास चला गया है। इस लोकतंत्र का मजाक बन गया है। धनिकों के पास बड़े-बड़े साधन है, बड़े स्कूल-कॉलेज, बड़े अखबार भारी-भरकम चुनाव कोष लेकिन गरीब जनता के पास या तो दान में मिली हुई जीवन है। या फिर भूख से मरना लिखा है। जब गरीब वर्ग थोड़े बहुत प्रयासों से झुकाने का प्रयास करते हैं तब लाल क्रांति होने लगती है। इस वक्त लोकतंत्र का हनन होने लगता है। मतपेटि का श्रमिकों के हाथ से निकलने लगती है। दलिय शासन कूड़े के ढ़ेर में फेंक दिए जाते हैं।[5] देश के आर्थिक जीवन का राज्य द्वारा नियोजित एवं नियंत्रित विकास मानवता को समाजवाद की सबसे बड़ी देन यह है कि वह सामाजिक प्रगति की प्रक्रिया को मनुष्य के प्रबुद्ध नियंत्रण और निर्देशन के अन्दर ले आता है। समाज में व्यक्तिवाद एवं स्वार्थ की प्रधानता रहने के कारण समाज की जो भी प्रगति हुई वह निरूद्देश्य हुई, उनकी न तो कोई योजना रही और उनका कोई सामाजिक लक्ष्य रहा। जिसकी प्राप्ति के लिए संगठित रूप से किसी ने प्रयास किया हो। समाजवाद मानव के भविष्य के लिए सामुहिक नियोजन ही वर्तमान अव्यवस्थित सामाजिक व्यवस्था के मुकाबले उसकी निर्विवाद श्रेष्ठता सिद्ध करता है। समाजवाद इतिहास का एक नया पृष्ठ खोलता है। जो समान रूप से भौतिक प्रगति एवं नैतिक तथा बौद्धिक विकास की दृिष्ट से नया होता है। नियोजित प्रगति की योजना का एक आवश्यक अंग है - नियोजित अर्थव्यवस्था किसी देश का आर्थिक संगठन उसके सम्पूर्ण जीवन की अमूल्य कुंजी है। अतः आर्थिक संगठन पर नियंत्रण तथा सामान्य लोक कल्याण बेहद जरूरी है। वर्तमान समय के आर्थिक संकट से सभी उबरने का पूरजोर प्रयास कर रहे हैं। समाजवादी नियोजन की सफलता के सामने पूंजीवादी नियोजन की विफलता का मुख्य कारण दोनों के बीच गंभीर विभेद है। जब तक लाभ कमाने की कोशिश जारी रहेगी। तब तक आम जनता का उद्धार संभव नहीं है। इस प्रकार के कठिन मार्ग से निकलने का एक मात्र उपाय है, समाजवाद।[6] आधारभूत एवं प्रमुख उद्योगों का समाजीकरण सामान्य जनता का राज्य आर्थिक क्षेत्र में वर्ग शासन के उन्मूलन पर ही आधारित होगा। सामान्य जनता की आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ है - व्यवसायिक सम्पत्ति के निजी स्वामित्व से उत्पन्न आर्थिक शोषण का अन्त। सामाजिकीकरण का अर्थ है, उत्पादन, विनिमय एवं वितरण के सभी साधनों को सामाजिक स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधीन लाना। इससे यह लाभ मिलेगा कि, सभी कारखाने तथा कर्मशालाऐं, सभी कच्चे माल, समस्त व्यापार, सारा बैंक तथा वित्त व्यापार समाज के हाथों में चला जायेगा। इन क्षेत्रों में अब किसी का निजी स्वामित्व नहीं होगा। केवल उद्योग ही नहीं बल्कि बैंक, परिवहन, बगान, खदान, सार्वजनिक सेवाऐं, बीमा आदि भी सामाजिक नियंत्रण के अन्तर्गत लाये जाने चाहिए। इसके तहत कारखानों के संचालन के लिए इस उद्योग में लगे हुए श्रमिकों के प्रतिनिधियों के सहयोग एवं राष्ट्रीय आर्थिक दृष्टि के अनुसार एक कपास उद्योग विभाग की स्थापना की जायेगी। समाजकृत मिलों में जो श्रम दास थे, वे समाज के शेष लोगों के साथ-साथ उन कारखानों में वे दिन-रात मजदूरी करते थे। इन कारखानों का संचालन एवं संगठन उनके हाथ में होगा। जिससे किसी प्रकार का अन्याय उनके साथ नहीं होगा। इससे उनकी मजदूरी पर भी बड़ा प्रभाव पड़ेगा। उनके लिए अच्छे मकान की सुविधा भी मिल जायेगी। उनके काम के घंटे कम किए जायेंगे। जिससे उन्हें लाभ ही प्राप्त होगा। इसमें कारखानें के मालिक भी श्रमिकों के साथ कार्य करेंगे। जिससे असमानता मिटेगी। जिस समाज का लक्ष्य सामाजिक समता है, वह शूरू से ही सम्पत्तिक विशेषताओं का निर्माण नहीं करेगा। इसके विपरित अगर कुछ कारखाने के स्वामी षडयंत्र रचने का प्रयास करेंगे। तब समाज में अव्यवस्था फैलने की संभावना होगी।[7] वैदेशिक व्यापार पर राजकीय एकाधिकार वैदेशिक व्यापार पर राजकीय एकाधिकार आर्थिक नियोजन का एक आवश्यक तत्व है। अर्थात् समाज ही निर्धारित करेगा कि उसे अपने राज्य से क्या आयात करना है क्या निर्यात करना है। लेकिन यही विचार व्यापारियों पर छोड़ दिया जाता है तब वे केवल समाज का अनिष्ट करेगा। मुनाफाखोरों के हाथों में वैदेशिक व्यापार समाज के लिए अलाभकारी सिद्ध होगा। उस स्थिति में मुद्रा एवं मूल्य को उत्पादन एवं खपत को नियंत्रित करना तथा औद्योगिक या कृषिक उत्पादन की किसी योजना के अनुसार सफलतापूर्वक कार्य करना कठीन होगा। सारी योजना ही अस्त-व्यस्त हो जायेगी। इन कठिनाईयों के अतिरिक्त निजी हाथों में वैदेशिक व्यापार के रहने से राष्ट्र के शत्रुओं के लिए चाहे वो देश के अन्दर हो या बाहर उसकी आर्थिक योजनाओं एवं कार्यकलापों को क्षतिग्रस्त होने की संभावना प्रबल हो जायेगी। वास्तव में वैदेशिक व्यापार राष्ट्रीय जीवन को इतने महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है कि ग्रेट ब्रिटेन जैसे बड़े देश जो स्वतंत्र व्यापार का अनुसरण करते थे, उन्हें भी विदेश व्यापार की व्यवस्था का परित्याग करना पड़ा।[8] आर्थिक जीवन के सामाजिकीकरण रहित क्षेत्र में उत्पादन, वितरण एवं ऋण संबंधी सहकारियों का संगठन सम्पूर्ण आर्थिक जीवन को एक ही बार में समाजिकृत नहीं किया जा सकता। इसके लिए अनेक छोटी-छोटी संस्थाऐं एवं व्यापार व्यक्तिक आधार पर ही चलते रहेंगे। इस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए ही उपर्युक्त बातों का अनुसरण करना आवश्यक है इसका उद्देश्य छोट-छोटे व्यक्तिगत व्यापार के स्थान पर सहकारी संस्थानों को प्रतिष्ठीत करना है। जिससे लघु उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सहकारी उपभोक्ता भंडार विकसित किए जायें। जो निजी भंडारों का स्थान ले लेंगे। एक सुसंगठित सहकारी संस्था अपने श्रेष्ठतर साधनों के बल पर विशेषकर अपने पीछे राज्य का समर्थन प्राप्त कर लघु व्यापार को पराजित करने में सदैव समर्थन प्राप्त होगी।[9] राजाओं और जमींदारों तथा अन्य सभी शोषकों का बिना क्षतिपूर्ति के उन्मूलन यदि राज्य का लक्ष्य हर प्रकार के शोषण एवं सामाजिक अन्याय से मुक्त एक ऐसे समाज का निर्माण करना है, जिसमें कोई वर्ग विशेषाधिकार वर्ग ना हो तो यह एक प्रगति का मार्ग होगा। एक अच्छा राजा अंत में राजा ही होता है, उसके प्रतिष्ठा के भाव सदैव जीवित रहते, थोड़े बहुत तौर पर वह प्रजा का शोषण अवश्य करता है, स्वतंत्र भारत में अगर राजतंत्र कायम रहा तब वह लोकतंत्र के लिए बाधक साबित होगा। पूर्व के काल में किसान अपनी उपज का एक हिस्सा राजा को देता था उस समय जमींदारी प्रथा नहीं थी लेकिन जमींदारी प्रथा आने से उनके शोषण में अत्यधिक वृद्धि देखी गई। क्योंकि भू-राजस्व की वसुली के समय जमींदार अपना मुनाफा भी रख लेता था। जिससे कृषकों पर अत्यधिक कर का बोझ पड़ता था, जमींदारी प्रथा के तहत् जमींदार निर्दयता के प्रतीक थे। भारत में भूमि उत्पादन का एक प्राथमिक साधन और जीवन निर्वाह का मुख्य स्त्रोत कृषि ही था। इस दौर में अत्यधिक जन संख्या वृद्धि के कारण कृषि पर निरन्तर बोझ बढ़ता गया। जिससे की दरिद्रता बढ़ती गई। इस दौरान महाजनों से ऋण लेकर कर का भुगतान करते थे। जिससे वे ऋणग्रस्तता के शिकार हो गए। इससे वे और गरीबी की दलदल में धंसते चले गए। किसानों के बीच भूमि का पुनर्वितरण किसानों के बीच भूमि का पुनर्वितरण करने से जिन किसानों के पास जमीन नहीं है उनके पास जीवन के साधन उपलब्ध हो जायेंगे। अभी कई किसानों के पास कई एकड़ जमीन है तो कई किसानों के पास भूमि की अत्यधिक कमी है। इस कारण किसानों में दरिद्रता छाई हुई है। यह असमानता उनके दुख का कारण बन जाती है। जब तक इन असमानताओं को हटाने की ओर ध्यान नहीं दिया जायेगा। गरीबी हटना मुश्किल है। वे निरन्तर शोषण के शिकार होते रहेंगे। राज्य द्वारा सहकारी एवं सामूहिक कृषि को प्रोत्साहन राज्य स्तर पर सामूहिक खेती को प्रोत्साहन देना होगा। वैसे भारत मुख्य रूप से कृषि प्रधान देश है। समाजवाद ही भारतीय कृषि को विनिष्ट और दिवालिया होने से बचा सकता है। यही भारतीय कृषि को समृद्धशाली और प्रगतिशील बना सकता है। अत्यधिक अनार्थिक जोतों में भूमि का विभाजन, निम्न उत्पादकता उद्योग कृषि शहर एवं गांव के बीच संतुलन का अभाव है, इसमें से एक से बढ़कर एक समस्या है। जिसे सुलझाना अति आवश्यक है। इसके लिए कृषकों के ऋणों की समाप्ति सभी जोतों का एकीकरण तथा सहकारी और सामूहिक कृषि, सहकारी ऋण बाजार की व्यवस्था, सहकारी सहयोग उद्योगों की स्थापना हो यह आवश्यक है। इसकी सफलता के लिए राज्य का मार्गदर्शन आवश्यक है। ऐसा संपन्न एवं सक्षम भूमिधारी कृषकों का निर्माण किया जाए जिसमें से प्रत्येक के पास अविभाज्य आर्थिक जोत हो और स्वतंत्रतापूर्वक अपनी भूमि पर खेती कर सके। सांस्कृतिक एवं नैतिक दृष्टि से कम विकसित मनुष्य होगा, जो अपने संकीर्ण व्यक्तिवाद को त्याग कर समाज के साथ एक रूप हो गया हो। किसान भी राष्ट्र का एक हिस्सा है। भारत में नियोजित विकास की आवश्यकता है क्योंकि यहां साम्राज्यवादी शासन के कारण भारत की अवस्था दयनीय हो गई है। जब तक कृषि व्यक्तिगत जोतों से बड़ी ईकाईयों में संगठित नहीं की जाती है। जब तक प्रत्येक गांव कृषि उत्पादन की ईकाई न बन जाए, तथा प्रत्येक ईकाई अन्य इकाइयों के साथ मिलजुलकर एक संगठित अर्थ रचना का अंग बन कर काम करने लगे। तभी यह संभव हो सकता है। राज्य कर निर्धारण द्वारा व्यक्तिनिष्ठ कृषि के अंतर्गत भी निश्चित फसलों को बढ़ा-घटा सकता है। इस प्रकार कृषि उत्पादन पर कुछ नियंत्रण स्थापित हो सकता है। जैसे कि रूस में प्रारंभिक दिनों में किया गया। यदि भारत की भूमि छोट-छोटे टुकड़ों में बंटी रहेगी और उन पर व्यक्तिगत खेती होती रहेगी। तब कृषि उत्पादन भी सीमित होगा।[10] कृषि एवं उद्योग को संतुलित करने के लिए कृषि समस्या का हल निकालना होगा। परन्तु इसके लिए भी सहकारी प्रयास और नियोजन की आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ ही सहकारी एवं सामूहिक कृषि को प्रोत्साहन दिया जाए उसका उन्नयन किया जाए। लेकिन जब तक औद्योगिक विकास अतिरिक्त ग्रामिण जनसंख्या को आत्मसात् नहीं कर लेता तब तक शायद बहुत सारे ट्रैक्टर फसल काटने के लिए यांत्रिक शेपर‘ और पुला बांधने के लिए वाइंडर हमें नहीं चाहिए। गांव में अगर विद्युतिकरण किया जाए और परिवहन के साधन उपलब्ध कराये जाये। तब गांव के कृषि का विकास संभव है। समाज के कुछ दुश्मन भी है जो कृषकों के बीच यह अफवाह फैलाते रहते हैं कि समाजवादी खेतिहरों से उनकी जमीन छीन लेंगे। लेकिन समाजवादियों का यह तर्क है कि, उनके पास ऐसा कोई टापू नहीं है, जहां इन किसानों की भूमि छीनकर उन्हें वहां ले जायेंगे। उनका कहना था, जिनकी जमीन है, उन्हीं की रहेगी। उस पर खेती भी वही करेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि, किसान उस जमीन पर खेती इस ढंग से करें कि समाज को अधिकतम लाभ प्राप्त हो। इसमें थोड़े व्यक्त्यिों का कल्याण नहीं होगा बल्कि समस्त समाज इसका लाभ उठा पाएँगे। यदि किसी भूमि को सभी लोग मिलकर कोड़ेंगे, बीज बोयेंगे, फसल उत्पादन करेंगे। तब उस जमीन पर सबका सम्मिलित रूप से अधिकार होगा। यह भारत की सम्पूर्ण आबादी के लिए बड़ा वरदान होगा। इससे गांव अपनी निम्न स्थिति से ऊपर उठकर समृद्धि की अवस्था तक पहुंच पाऐगा। आधुनिक शहर मानवीय बस्तियों के रूप में दानव तुल्य है। उनकी जनसंख्या उनके परिवहन के साधन, अस्वच्छता, उनकी गंदी बस्तियां हमारे मन को झकझोर देती है। शहर अपने अधिकांश निवासियों के लिए भयानक वास स्थल है। इनकी नाट्शालाऐं, मनोरंजन गृह, आत्मा को पोषण देने वाली, मन को आनंद देने वाली सौंदर्य की वस्तुएंे नहीं है, बल्कि मस्तिष्क तथा थके हुए शरीर कष्टहरण करने वाली दवाओं के तुल्य है।[11] इसके अलावे आधुनिक शहर केवल ग्रामिण जनता के ही नहीं बल्कि शहर की श्रमिक जनता के भी शोषण पर पनपे हैं। इस शोषण से उत्पन्न परिस्थिति शहर और गांव के बीच अस्वाभाविक विरोध पैदा करती है जिसमें गांव हमेशा घाटे में रहता है। एक ओर जहां कला, ज्ञान, विलास एवं सुख के साधन शहरों में मौजूद हैं वहीं गांव उपेक्षित एवं अविकसित रह जाते हैं। जो शहरों तथा गांव के बीच वैमनस्य पैदा करने का काम करते हैं। समाजवाद का मुख्य लक्ष्य सम्पूर्ण समाज का समन्वित तथा संतुलित विकास करना है। समाजवाद मानव को किसी भी तरह से कष्ट नहीं पहुंचाऐगा। समाजवाद के अंतर्गत शहरों का निर्माण योजनाबद्ध रीति से होगा। जिसके तहत केन्द्रीयकरण का निवारण किया जायेगा। क्योंकि उद्योग विकेन्द्रीत होंगे। भौगोलिक के साथ-साथ संख्यात्मक योजना भी होगी। दूसरी ओर जो गांव अभी दुनियां से अलग-थलग है, जो छोटे-छोटे घरों के झुण्ड में सिमटे हुए हैं। वे प्रगतिशील समुदायों में परिवर्तित हो जायेंगे। शहर के समाज गांव भी उत्पादन की औद्योगिक ईकाई बनेगा। उसका अपना शासन होगा। अपना विद्यालय होगा अपने मनोरंजन केन्द्र तथा अपना संग्रहालय भी होगा।[12 ] श्रम करने या पोषण पाने के अधिकार की राज्य द्वारा मान्यता जब तक परती भूमि पड़ी हुई थी, शारीरिक शक्ति सम्पन्न व्यक्त्यिों को सुरक्षा की आवश्यकता भी नहीं थी। लेकिन जब भूमि दुर्लभ हो गई वह उपलब्ध नहीं हो पाती थी और रोजगार भी उपलब्ध नहीं हो पाता था। तब लोग या तो भूखे रहते थे या फिर लुट-पाट करते थे। लूट-पाट करने वालों को तो पकड़कर न्यायालय तक ले जाया जाता था। तब उनके साथ न्याय होता था। लेकिन जो भूखे मर जाते थे, उनकी आत्मा को तो बस ईश्वर की ही कृपा प्राप्त होती थी।[13] आज के युग में रोजगार की समस्या काफी बड़ी हो गई है। उद्योगवाद ने श्रमिकों उनके श्रम बेचने पर मजबूर कर दिया है। जिसके बल पर वे जीवित रहते हैं जब औद्योगिक संकट के कारण बेरोजगारी का जन्म हुआ। तब श्रमिक लड़ाकु बन गया इसी वक्त आधुनिक राज्यों ने बेरोजगारी बीमा की व्यवस्था जो आज किसी न किसी रूप में बेरोजगारी भत्ता ‘मईया योजना‘ ‘पेंशन योजना‘ के रूप में दिया जाता है। भारत में साम्राज्यवाद के अधीन उद्योग और कृषि दोनों पंगु हो गए हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि बड़े स्तर पर बेरोजगारी समस्या खड़ी हो गई है। समाजवादी ऐसी परिस्थिति से उबरने का मार्ग ढूढ़ते हैं, उन्हें इस बात की चिंता है कि अपने ही देश के वासी अपने देश में ही पराये हो गए हैं। समाजवाद के समाजवादियों का यह पहला कर्तव्य होगा कि यहां के लोगों को रोजगार प्रदान करें।[14] आवश्यकता के अनुसार दाम एवं योग्यता के अनुसार काम समाजवाद ने जिस तरह के लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उसके तहत् कारखानों में खेतों-खलियानों में, विद्यालयों प्रयोगशालाओं नाट्यशालाओं में पूरी ताकत से काम करेगा। जो उनके पास उपलब्ध होगा, उससे अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर लेगा। अपनी आवश्यकता के अनुसार वह उपभोग की वस्तुऐं जैसे वस्त्र, अन्न, पुस्तकें जब निर्मित करेगा। तब कुछ अपने लिए भी रख लेगा। बाकि वस्तुओं को बाजार में ब्रिकी करके धम अर्जन करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य हैं, उपभोग की प्रत्येक वस्तु काफी प्रमाण में प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपलब्ध हो सके। जब तक उस अवस्था तक नहीं पहुंचते जहां सभी के लिए सामग्री उपलब्ध हो सके। तब तक राशनबंदी की प्रत्यक्ष पद्धति से या वेतन निर्धारण की अप्रत्यक्ष पद्धति से उपभोग पर नियंत्रण रखना होगा। ऐसी अवस्था में नए प्रकार से मानव का चरित्र निर्माण हो चुका होगा। इस वक्त कोई अपराध करेगा तो उसे समाज ही हेय दृष्टि से देखेगा। वे स्वतंत्रता का सही लाभ उठा पाऐंगे। उस समाज में जीवन की एवं काम की पूर्ण सुरक्षा तय होगी। यथा-बुढ़ापे, बीमारी एवं प्रसूति-काल के लिए पूर्ण व्यवस्था होगी। किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की बात की चिंता नहीं होगी। केवल इसी बात पर विशेष ध्यान देना होगा कि वह अच्छा मनुष्य कैसे बन सकता है। उसे वस्तुओं के केवल निर्माण एवं वितरण की चिंता होगी। उस समय किसी धन-संग्रह करना भी उसे अन्यायोचित लगेगा। वह समाज से जो भी वह प्राप्त कर सकेगा। ऐसा भी नहीं होगा कि आज ये वस्तुऐं हैं, कल लोप हो जायेगा। पूर्ण सुरक्षा की भावना संग्रह की प्रवृत्ति को समाप्त कर देगी। उस समय तक मुद्रा एवं मजदूरी तथा व्यक्तिगत आय में कुछ भेद नहीं रहेगा। वस्तुओं के उत्पादन पर विनियोजित राशि तथा सामाजिक सुख-साधनों की व्यवस्था पर व्यय के अनुपात में मजदूरी में भी वृद्धि होती रहेगी।[15] व्यवसायिक पर व्यस्क मताधिकार लोक प्रतिनिधित्व क्षेत्रिय आधार पर न होकर व्यवसायिक आधार पर होगा। अतः व्यवसायिक प्रतिनिधित्व अधिक वास्तविक प्रतिनिधित्व होगा। व्यवसाय विविध रूपों में होने के बावजूद लोगों में एकता की भावना बनी रहेगी। इसमें सबका हित शामिल होंगे। जिससे भेद-भाव नहीं पनपेगा। वर्गहीन समाज के पूर्व विकास के साथ-साथ राज्य स्वयं अपने आधुनिक अर्थ में क्षीण होकर समाप्त हो जायेगा। उस स्थिति में लोक प्रतिनिधित्व राज्य की राजनीतिक सभाओं के लिए नहीं बल्कि उद्योग-पार्षद, शिक्षा पार्षद तथा अन्य संस्थाओं के लिए होगा। यदि हम महान भारत की कल्पना करते हैं तब यह सही कदम होगा। जिनके सहारे हम अपने सपने को साकार कर सकते हैं। अगर भारत से हम गरीबी अन्याय गंदगी आलस्य, अज्ञानता को दूर भगाना चाहते हैं तो यह सही कदम है, समाजवाद के निर्माण से हमारे कार्य में सदैव उन्नती होती रहेगी। अंग्रेजों ने जब रेल-तार बिछाये, बैंक तथा मिल और मालगोदाम खड़े किए तो उनके मार्ग में भारत का पिछड़ापन बाधक सिद्ध नहीं हुआ। आधुनिक परिस्थिति में विज्ञान एवं उसके आविष्कारों के सहारे, समाजवाद का निर्माण हम करना चाहे तो कहीं भी कर सकते हैं।[16] भारत में कोई व्यक्ति या फिर दल साम्राज्यवाद से अधिक शक्तिशाली नहीं है और यदि हम उसे पराजित कर देते हैं तब हमारे संकल्प को चुनौती देने वाली कोई शक्ति नहीं होगा। ये राजे-महाराजाऐं काफी शक्तिशाली दिखते हैं, जिनके पास अपना कुछ भी नहीं है, इन्होंने जो भी अर्जन किया है। यहीं के जनता, जमीन से। जब समाजवाद का संचार हो जायेगा। तब इनकी साम्राज्यवादी शक्ति धरासायी हो जायेगी। समाजिक समाजवाद ने मनुष्य जाति के सामने समता, स्वतंत्रता, बन्धुता, शांति एवं अंतर्राष्ट्रीय भ्रातृत्व के श्रेष्ठ आदर्श उपस्थित किए हैं। जब समाजवाद की स्थापना समाज में हो जायेगी। तब एक नए समाज का निर्माण होगा। समाजवादी समाज का निर्माण मूलतः एक नये प्रकार के मनुष्य का निर्माण है। अब तक समाज परिवर्तन का गति विज्ञान स्वार्थों का संघर्ष रहा है। स्वार्थ से प्रेरित होकर श्रमिक एक भिन्न समाज व्यवस्था का निर्माण करना चाहता है। जब तक व्यक्ति का नैतिक विकास हो नहीं जाता वह स्वेच्छा से अपने मानव बन्धुओं के हीत में अपनी आवश्यकता एवं स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए तैयार रहें। जब तक व्यक्ति आत्मसंयम का पाठ नहीं सीखता तब तक वह संयम पर आधारित जीवन नहीं जी सकता। सांस्कृतिक सांस्कृतिक तौर पर भी मानव को अपने विकास की बात सांेचनी होगी। भारतीय संस्कृति अन्य संस्कृतियों से काफी भिन्न है। हमारी संस्कृति में मानव का उत्थान नीहित है। अगर कुछ कुरूतियों को हटा दें, जो हमारे मार्ग के अवरोधक हैं तो हमें अपनी संस्कृति से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। जिस प्रकार हमारे संस्कृति में मानव -मानव से प्रेम, बन्धुता, नैतिकता का समावेश है, अगर उस राह पर भी हम चलें तो समाजवाद का निरन्तर विकास होता रहेगा।[17] बौद्धिक बौद्धिक क्षेत्र का ज्ञान हमारे प्राचीन ग्रंथों से प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो जाता है। जो हमारी संस्कृति को संजोये हुए है। जिससे मानव अछुता नहीं रह सकता। शैक्षणिक भारत पूर्व के काल से ही शिक्षा की दृष्टि में उत्कृष्ट रहा है। उस समय भी कई बड़े विश्वविद्यालय थे, जिनमें विदेश से भी छात्र पढ़ने आते थे, आज भी मनुष्य जो पिछड़ गए हैं। उन्हें शिक्षित करने की आवश्यकता है। तभी वे समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। शिक्षा के नये अवसर रोजगार को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होंगे। जिससे समाज में असमानता मिटेगी। इसके साथ ही नये कीर्तिमान स्थापित करने वाले मनुष्य के कार्य समाज को लाभान्वित करेंगे। समाज को जिसकी नितांत आवश्यकता है। अध्यात्मिक भारत का अध्यात्मिक क्षेत्र में अटूट विश्वास है। जिस पर आधारित वह जीवन को जीता है। इससे मनुष्य का चरित्रिक पतन नहीं होता। वे अच्छे कार्य करने में संलग्न रहते हैं। अध्यात्म से मनुष्य के नैतिकता का विकास होता है। मनुष्य को समाज से जुड़े रहने के लिए नैतिक रूप से उसे सबल होना आवश्यक है। |
||||||
| निष्कर्ष |
उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि जयप्रकाश नारायण ने सम्पूर्ण क्रांति के माध्यम से समाज को एकजुटता प्रदान की। जिससे भारत के लोगों का विकास निरन्तर होता रहे। वे अपने भारतीय बन्धुओं की परेशानियों में बाधक न बने तथा उनमें एकता बन्धुता की भावना का विकास होता रहे। |
||||||
| सन्दर्भ ग्रन्थ सूची |
|
||||||