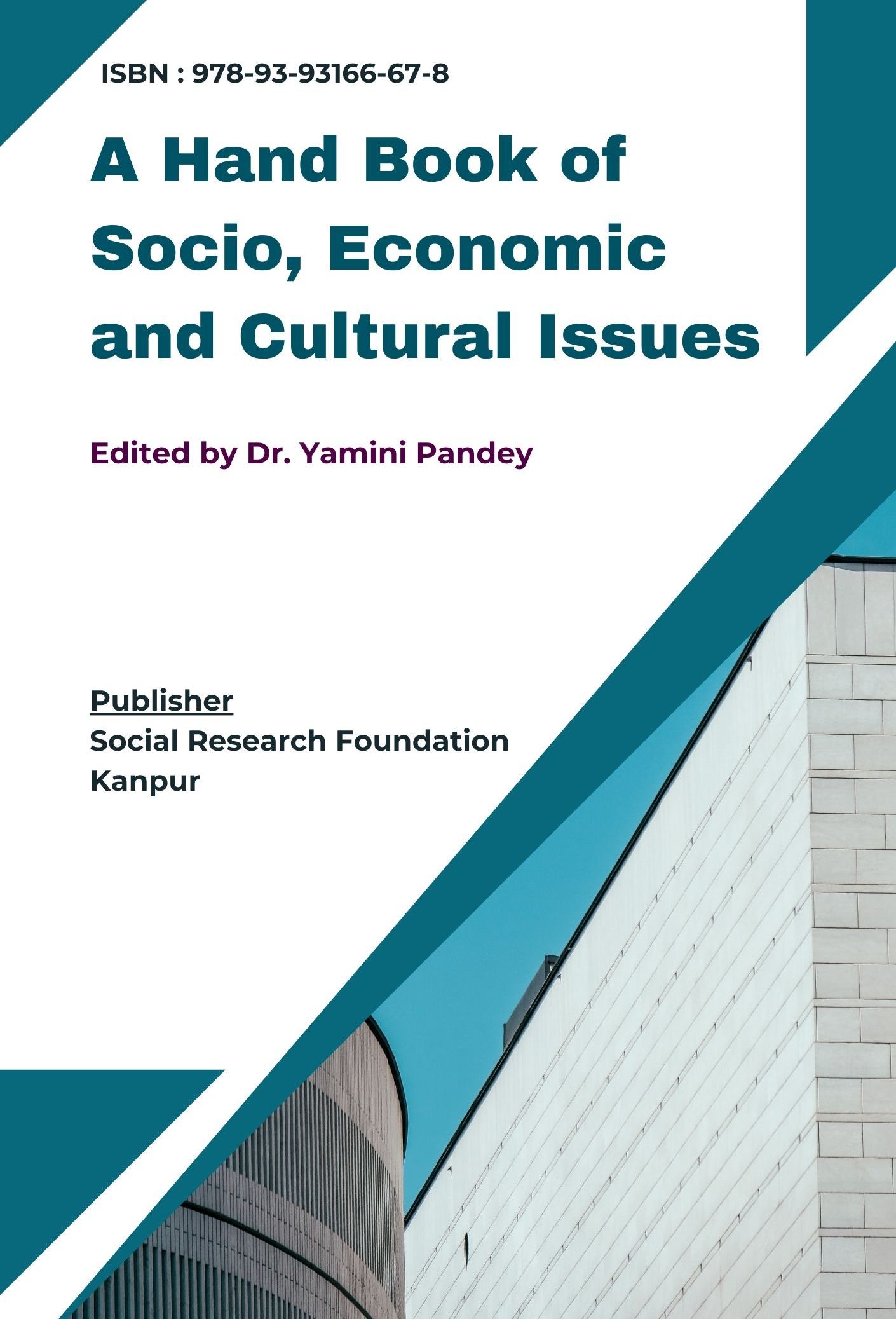 |
| A Hand Book of Socio, Economic and Cultural Issues ISBN: 978-93-93166-67-8 For verification of this chapter, please visit on http://www.socialresearchfoundation.com/books.php#8 |
बस्तर के भूमकाल का महान योद्धा गुण्डाधूर |
|
डॉ. पूजा शर्मा
सहायक प्राध्यापक
इतिहास विभाग
शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय
बिलासपुर छत्तीसगढ़, भारत
|
|
DOI:10.5281/zenodo.15100974 Chapter ID: 19898 |
| This is an open-access book section/chapter distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. |
स्वतंत्रता के पूर्व भारत में जनजातीय विद्रोह एक महत्वपूर्ण घटना थी, जो मुख्य रूप से राजनीतिक या वैचारिक कारणों के बजाए आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से प्रेरित थी। अधिकतर इसका उद्देश्य अपनी परंपरागत सांस्कृतिक जीवन शैली को बनाए रखना था। आदिवासी विद्रोह की प्रकृति स्थानीय, स्वतः स्फूर्त सीमित क्षेत्र में और घटनाओं और व्यक्ति प्रेरित थी। इनका प्रभाव सरकारी इमारतों और वस्तुओं पर हुआ। इनके विरोधी जमीदार, साहूकार, व्यापारी और मिशनरियां थी। ब्रिटिश सरकार के आधुनिक अस्त्र-शस्त्र एवं यातायात संचार के साधन के सामने ये परंपरागत तीर, धुनष, भाले, कुल्हाड़ी के प्रयोगकर्ता सीधे सादे आदिवासी अत्यंत उग्र, उत्साही और हिंसक भी हुए। बस्तर के गुण्डाधूर को इसी प्रकार का आदिवासी विद्रोही माना जाता है जिसमें सैन्य संगठन की क्षमता और साहस कूट-कूट कर भरा था। ब्रिटिश शासन काल में बस्तर रियासत 1300 वर्ग मील क्षेत्र में फैली एक बड़ी रियासत थी। बस्तर के उत्तर में कांकर, दक्षिण में गोदावरी भद्राचलम पश्चिम में चांदा व निजाम का शासन था। इस रियासत को बस्तर का नाम बांसों के उपवन के रूप में दिया गया था। नल, नाग एवं काकतीय वंश के शासको ने बस्तर को अत्यंत समृद्ध एवं विस्तृत बनाया।[1] बस्तर मूलतः एक आदिवासी क्षेत्र है, विशाल प्राकृतिक संपत्ति के स्वामी यहां के आदिवासी अपने अज्ञानता के कारण पिछड़े रहे, बाहरी अंग्रेजों ने इनको ठगा और उनके इतिहास को दफन कर दिया। ग्रीक्सन ने 1938 में इसे भारतीय इतिहास का ‘बैकवाटर’ कहा। बस्तर के आदिवासियों का इतिहास अक्षरशः क्रांति का एक ऐसा इतिहास है, जिसमें बड़े और विविध पैमाने पर घटनाओं की भरमार है।[2] ब्रिटिश शासन के दौरान बस्तर में कई विद्रोह हुए इनमें हल्बा विद्रोह, तारापुर, भोपालपटृनम, परलकोट, मरिया, मुड़िया, कोई विद्रोह, रानी चोरिस का विद्रोह एवं भूमकाल प्रसिद्ध है। बस्तर के आदिवासी विद्रोह के इतिहास में 1910 का भूमकाल विद्रोह प्रसिद्ध है। यह विद्रोह बस्तर की आजादी की लड़ाई में प्रमुख स्थान रखता है। इसे भूमकाल या लाल विद्रोह के नाम से जाना’ जाता है। भूमकाल का अर्थ है ‘लोगों का एक स्थान पर जमा होना और शीघ्रता से चले जाना इस विद्रोह में बस्तर के निवासी धुरवा, परजा, भतरा, मुड़िया, मडिया, हल्बा, धाकड़, महारा आदि आदिवासी समुदायों ने भाग लिया था।[3] बस्तर के एक विस्तृत क्षेत्र में फैला यह आदोलन अत्यंत उग्र और प्रभावशाली था। भूमकाल आंदोलन का कारण ब्रिटिश शासन द्वारा राजा की अधिकारों को योजनाबद्ध तरीके से घटाया जाना था। दीवान बैजनाथ पंडा को प्रमुख बनाया गया, राज परिवार के लाल कलिंदार सिंह की योग्यता महत्वाकांक्षा और ब्रिटिश विरोधी नीति, राजा भैरमदेव की अक्षमता, रानी स्वर्ण कुंवर की उपेक्षा, राजा रूद्र प्रताप देव से असंतोष आदि इस विद्रोह के राजनीतिक कारण थे।[4] वनों को आरक्षित किए जाने के कारण आदिवासी असंतुष्ट थे। स्थानांतरित कृषि की मनाही, वन उपज ले जाने की मनाही, बिना मुआवजा भूमि छीन लेना, अंग्रेजी स्कूल में आदिवासियों को जबरदस्ती प्रवेश लेने के लिए बाध्य करना, प्रतिष्ठा की हानि, सरकारी दुर्व्यवहार, बेगारी और बेरोजगारी, ठेकेदारी एवं साहूकारी आदि इस विद्रोह के लिए व्यापक रूप से उत्तरादायी कारण थे। बस्तर के असंतुष्ट आदिवासियों ने 1910 में ब्रिटिश साग्राज्य और बस्तर रियासत के विरूद्ध सशस्त्र विद्रोह किया। स्कूल भवन, थाना, वन कार्यालय, काजी हाउस जला दिए गए, दुकानों और बाजारों को लूट लिया गया, लाल कलिंदर सिंह गुंडाधुर और रानी स्वर्ण कुंवर के नेतृत्व में यह विद्रोह बड़े पैमाने पर फैला, वन कर्मचारियों को मारा गया, तार लाइन लाइनों को काट दिया गया गया, पूसपाल, दंतेवाड़ा, भैरसमगढ़ के इलाकों में इस विद्रोह का स्वरूप अत्यंत व्यापक था। सरकार ने कठोर दमन चक्र चलाएं, कई गांव क्रूरता से जला दिए गए, गोली चालन में 39 आदिवासी मारे गए, सैकड़ो घालय हुए 44000 रू. का अर्थदण्ड लगाया गया, 200 पुलिस सेंट्रल प्रोविंसेस से 150 मद्रास प्रेसीडेंसी से और 170 अन्य स्थानों से बस्तर में लगा दिए गए। लाल कलिंदर सिंह, स्वर्ण कुंवर एवं अन्य 15 को गिरफ्तार कर लिया गया।[5] इस प्रकार यह विद्रोह फरवरी में प्रारंभ हुआ और मई 1910 तक पूर्णता समाप्त हो गया। यह विद्रोह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया। जब बस्तर ब्रिटिश राज के अधिकार में था, उसे समय प्रत्येक आदिवासी में यह एक खास प्रवृत्ति थी कि वह विजेताओं से संघर्ष कर जननायक बन जाए। यह आत अनेक उदाहरणों में देखने को मिलती हैं। पिछले दो शताब्दियों की आदिवासी कविताओं में ऐसे गुमनाम लोगों की चर्चा की गई है, जो विदेशी अत्याचारों के खिलाफ अपने लोगों के लिए लडे थे, उनमें से एक महान गुंडाधूर भी था जो अंतिम समय तक ब्रिटिश सरकार की अधीनता को अस्वीकार करता रहा, सरकार के शरण में जाने के बजाय वह बीहड़ वनों की शरण लेता हैं, बस्तर में एक गुंडाधूर है जो अकेला लड़ता है और अंग्रेजों की समूची सेना द्वारा डराए जाने पर भी हथियार नहीं डालता, और गेयर जैसे सर्वोच्च मिलिट्री अधिकारी पर प्रहार करने का साहस रखता है। एक ऐसा गुंडाधूर बस्तर का महानायक जो तीन दिन और रात बिना भोजन पानी के बिता देता है, जब बाहर आता है तो ब्रिटिश सेना से भिड़ जाता है।[6] गुंडाधूर के विषय में इस प्रकार की जानकारी से प्रमाणित होता है कि वह आदिवासी विद्रोह की स्वतः प्रेरणा से प्रभावित था। उसका आंतरिक बल इतना मजबूत था कि ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीतियां उसे विचलित नहीं कर पायी। वह बार-बार गिरकर उठाखड़ा होता था। बस्तर में भूमकाल के लिए पहले से योजना बनाई गई थी। रईस, राजमान्य एवं जनसामान्य की बैठक बख्शी की हवेली में हुआ करती थी। इससे जनअसंतोष को बल मिलता था वीर सिंह बैदर, जो गढ़िया ग्राम के मालगुजार थे, ने गुंडाधूर को धुरवा लोगो को तैयार करने की जिम्मेदारी दी थी। लाला जगदलपुरी ने लिखा हे कि गुंडाधूर धुरवा नेता थे, जिनकी क्रांति प्रतिभा इन्हीं बैठकों में सक्रिय हुई। गुंडाधूर और लाल कलिंदर सिंह दोनों तांत्रिक थे, दोनों में प्रगाढ़ मैत्री थी। उलनार गांव में मडिया धुरवा क्रांतिकारी लाल मिर्च बंधी आम की टहनियों ‘डार मिरि’ लेकर प्रचार के लिए निकलते थे।[7] गुंडाधूर ने धुरवा आदिवासियों को संगठित कर विद्रोही खेमा तैयार किया था, जिसका उपयोग ब्रिटिश सैनिकों को खदेड़ने में किया गया था। गुंडाधूर के विद्रोह की शुरूआत जगदलपुर से हुई धीरे-धीरे यह अन्य क्षेत्र कोंडागांव, अंतागढ़, नारायणुपर, दंतेवाड़ा, और कोंटा तहसील तक फैल गई। 1 फरवरी से 15 फरवरी तक जगदलपुर विद्रोहियों को कब्जे में रहा, लेकिन गेयर ने आदिवासियों को विश्वास में लेकर शांत कर दिया। 16 फरवरी को इंद्रावती नदी के खड्ग घाट पर व्यापक युद्ध हुआ, यह 6 घण्टे का निर्णायक युद्ध था, इसमें 25000 लोग मारे गए। गुंडाधूर ने वीरता का परिचय दिया, लेनिक पराजय से विद्रोहियों का मनोबल गिरने लगा था। इसमें लाल कलिंदर सिंह को भी गिरफ्तार किया गया था। 25 फरवरी को जबलपुर, विजगापत्तम, जयपुर तथा नागुपर से सैन्य दल बस्तर पहुंच गए।[8] इन परिस्थितियों में गुंडाधूर के लिए मुश्किल था कि वह सेना संगठित करे, उसने अन्यत्र विद्रोह का नेतृत्व करना प्रारंभ किया। गुंडाधूर ने अलनार गांव की टेकरी को अपना शिविर बनाया। अलनार में रहकर उसने फिर से सामरिक गतिविधियां प्रारंभ कर दी। लोगों को फिर से एकजुट करने लगा, धीरे-धीरे एक विस्तृत क्षेत्र में गुंडाधूर के सैन्य दल के आक्रमण तेज होने लगे, सैन्य दल में सम्मिलित सभी युवाओं का यह आक्रोश था कि जगदलपुर में ब्रिटिश सेना के आने के साथ ही अंग्रेज अधिकारियों के खेमे में परिवर्तन हो गया। आदिवासियों पर अत्याचार से विद्रोह की आग और भड़क गई गुंडाधूर ने उन्हें संगठित की करने का कार्य किया गुंडाधूर ने पूर्वी क्षेत्र पर तब तक नियंत्रण स्थापित कर लिया था एवं अलनार गावं की सुरक्षा के पूरे उपाय कर लिए थे। गुप्तचरों से सूचना प्राप्त कर गेयर ने अचानक रातों-रात धावा बोल दिया, आदिवासियों ने आत्मसमर्पण के स्थान पर युद्ध चुना, तीरों की बौछार प्रारंभ कर दी, इस बार उनका नारा था ‘हम युद्ध करेंगे’ लेकिन गेयर की फौज की गोलियों के सम्मुख धनुष-बाण-भला कब तक टिक सकता था, बड़ी संख्या में विद्रोही मारे गए।[9] लेकिन गुंडाधूर अगली कार्यवाही के लिए तैयार थे, उन्हें बार-बार पराजय मिली लेकिन फिर से सेना संगठित कर आगे बढ़ते रहे। 28 फरवरी 1910 तक पुलिस और सैन्य दल बस्तर के सभी दिशाओं में फैल चुके थे सैकड़ो आदिवासी गिरफ्तार हुए। 25 मार्च 1910 को गुंडाधूर ने पूर्णिमा की अर्थ रात्रि में नेतानार में 600 मडिया दल के साथ गेयर और उसकी सेना पर आक्रमण कर दिया, वे विजयी हुए और जश्न मनाते रहे, लेकिन उनके सहयोगी सोनू माझी ने गद्दारी की, उसके अंग्रेज अधिकारियों को सूचना दी, ब्रिटिश सैनिकों ने शिविर में गोलियों की बौछार कर दी। इसमें 21 आदिवासियों मारे गए और सैकड़ो घायल हुए। गुंडाधूर के सहयोगी डेबराधूर और अन्य सैनिकों को भी गिरफ्तार कर लिया गया और जगलदपुर में फांसी दे दी गई। गुंडाधूर जंगल की ओर भाग गए, बाद में उसके बारे में और अन्य जानकारी नहीं मिलती कि उसका अंत किस प्रकार हुआ अंग्रेज अंत तक उसे ढूंढते रहे लेकिन पकड़ नहीं पाए।[10] एक अन्य स्त्रोत के अनुसार गुंडाधूर एवं डेबराधूर को पकड़ने के लिए सरकार ने क्रमशः 100000 और 5000 का इनाम घोषित किया था, किन्तु यह प्रयास भी असफल रहा।[11] स्पष्ट है कि ब्रिटिश सराकर के लिए भूमकाल का सबसे बड़ा विद्रोही गुंडाधूर था। जिसकी उत्पादी गतिविधियाँ ब्रिटिश सरकार को परेशान कर रही थी। अंग्रेजों का मानना था कि एक बार यदि गुंडाधूर को पकड़ा लिया जाए, तो आगे के विद्रोह अधिकार तीव्र एवं प्रभावशाली नहीं होंगे। तीन माह तक चला यह संघर्ष पूर्ण सफल नहीं हो पाया, ब्रिटिश सरकार ने कठोरता पूर्वक इसका दमन कर दिया। अस्त्र, शस्त्र, संगठन, आधुनिक यातायात एवं संचार के साधन, नेतृत्व, आदि सभी दृष्टियों के ब्रिटिश सरकार अधिक शक्तिशाली थी।[12] आदिवासियों को विद्रोह के लिए संगठित करना, सरकारी दमन को झेलना, राजा का विरोध सहन करना और अपने साथियों का विश्वास घात प्राप्त होना आदि के साथ यदि तीन माह तक सक्रिय संघर्ष चला, तो यह एक उपलब्धि ही मानी जाएगी। उपनिवेशवाद के खिलाफ गुंडाधूर ने जो जंग छेड़ था, उसकी यादें बस्तर के आदिवासियों को आज भी हैं। सीतापुर, नेतापुर, अलनार, कांडानार, आदि गांव के धुरवा लोगों की भुजाएं उसकी याद में आज भी फड़क उठाती है। बस्तर की माताएं आज भी गुंडाधूर को ‘रॉबिनहुड’ के रूप में याद करती है। कुछ लोग तो उसमें अनंत जादुई शक्तियों का भंडार मानते थे। उसके लड़ते समय, उसके तलवार चलाते समय, मुंड के मुंड कट जाते थे, और बस्तर की समूची धरती परदेसियों के खून से लहू लुहान हो जाती थी।[13] ‘गुंडाधूर चो लड़तो बेरा खान्डा चो धार पड़तो बेरा मून्डी ऊपर धड़ पड़ेसे लड़ाई लडून सरतो बेरा लहु चो टार धडेसे। गुंडाधूर की कथा बहुत संक्षिप्त है और चरित्र भी लब्धप्रतिष्ठित नहीं है, किन्तु सभी चरित्रों में एक ‘विद्रोही भाव’ है, एक ‘वीर भाव’ है और यह ‘वीर भाव’ उसे महान भूमकाल में उनकी आहुति के कारण पैदा हुआ है। एक महान कार्य को उन्होंने पूरा किया था। ब्रिटिश राज के प्रति उनकी साहसपूर्ण चुनौती उन्हें महान बनाती है। यह देशभक्त लोग थे जिन्होंने अपनी जन्मभूमि की स्वतंत्रता के लिए खुशी-खुशी बलिदान दे दिया था लोकगीतों में उन पर विश्वास और आत्म सम्मान झलकता है।[14] आदिवासी इतिहास लेखन में इन लोकगीतों और कथाओं का विशेष महत्व है। लाला जगदलपुरी ने अपनी पुस्तक में इन लोककथाओं के बारे में विस्तृत विवरण दिया है मौखिक पंरपरा में अब भी गुंडाधूर की स्थान अमर है। बस्तर का भूमकाल 1910 में ही समाप्त हो गया। इसने ब्रिटिश शासन को सीमित रूप से ही प्रभावित किया। ब्रिटिश सरकार की कुशल शक्ति और गुप्तचर व्यवस्था के कारण विद्रोह का दमन आसानी से कर दिया गया। गुंडाधूर जैसे योद्धा को अपने ही लोगों के बीच विश्वास घात, दलबदल, विघटन और पराजय का सामना करना पड़ा। गुंडाधूर तत्काल या अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाए। लेकिन गुंडाधूर ने आदिवासियों समाज और संस्कृति को व्यापक रूप से प्रभावित किया। गुंडाधूर के लोगों की जान, सम्पत्ति और संसाधनों का बालीदान व्यर्थ नहीं गया। गुंडाधूर ने अपने कृत्यों से आदिवासी समाज को नवीन विचार, उत्साह, साहस और चुनौतियों से अवगत कराया। आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्वकर्ताओं ने केवल आदिवासी मुद्दों को स्वीकार किया बल्कि उनके बलिदान, साहस और दृढ़ता की सराहना भी की। संदर्भ ग्रंथ:-
|