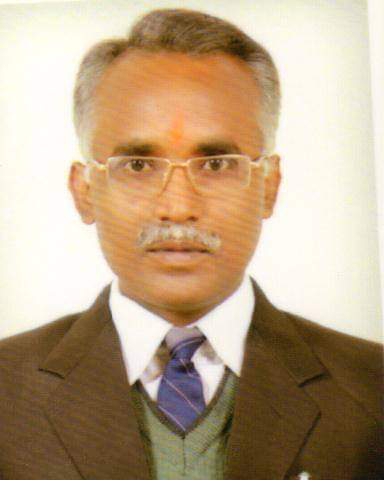|
|||||||
|
भारतीय सन्दर्भ में बालश्रमिकों का अध्ययन: दशा एवं दिशा |
|||||||
| Study of Child Labor in Indian Context: Status and Direction | |||||||
| Paper Id :
18522 Submission Date :
2024-02-03 Acceptance Date :
2024-02-09 Publication Date :
2024-02-25
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. DOI:10.5281/zenodo.10670580 For verification of this paper, please visit on
http://www.socialresearchfoundation.com/anthology.php#8
|
|||||||
| |||||||
| सारांश |
बालश्रमिक,
श्रमिकों में एक ऐसा वर्ग है
जोकि अपने विकास की मूलभूत सुख सुविधाओं से वंचित होता रहा है जैसे शिक्षा,
स्वास्थ्य,
बौद्धिक,
शारीरिक,
सामाजिक इत्यादि। राष्ट्रीय
एवं अंतर राष्ट्रीय स्तर पर अनेकों विधियां इस वर्ग के संरक्षण के लिए निर्मित की
गई है और कई आंदोलन भी संस्थाओं और
व्याक्ति विशेष द्वारा संचालित कर के समय
समय पर इस वर्ग का संरक्षण व संवर्ध किया जाता रहा है भारत के परिपेक्ष में भारतीय
न्यायालयों की भूमिका अविस्मरणीय है न्यायमूर्ति पी0एन0 भगवती तथा आर0एस0 पाठक ने यह विचार व्यक्त किया कि आज के
बालक कल के नागरिक है, उन्हीं के कंधों पर कल के भारत का भार है उन्हीं,
पर राष्ट्र की गरिमा और विकास
निर्भर है। |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सारांश का अंग्रेज़ी अनुवाद | Child labor is a class of workers which has been deprived of the basic amenities of development like education, health, intellectual, physical, social etc. Many laws have been made at the national and international level for the protection of this class and many movements have also been conducted by institutions and individuals to protect and promote this class from time to time. In the context of India, the Indian courts have the role is unforgettable. Justice PN Bhagwati and RS Pathak expressed the view that today's children are the citizens of tomorrow, the burden of tomorrow's India rests on their shoulders, and the dignity and development of the nation depends on them. | ||||||
| मुख्य शब्द | बाल श्रमिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक। | ||||||
| मुख्य शब्द का अंग्रेज़ी अनुवाद | Child labour, Education, Health, Intellectual, Physical, Social. | ||||||
| प्रस्तावना | संसार के प्रायः सभी समाजों की अपनी-अपनी विशेषताएँ है, कुछ खूबियाँ कुछ खामियाँ है। इस पृथ्वी का शायद ही कोई समाज ऐसा होगा जो समस्याविहीन एवं कठिनाईयों से मुक्त हो। ‘बचपन में बचपन को मोहताज’ ईश्वर के बनाये इस समाज का भी गजब का चरित्र है। जीवन में बचपन से सुखी कोई बहुमूल्य जीवन नहीं हो सकता है। किसी के जीवन का सबसे सुखद अनुभव बचपन ही होता है जिसके गुजरने के बाद मनुष्य चाहता है कि कास एक बार और ये मिल जाता तो जिस चीज की कमी बचपन में अधूरी रह गयी उसकी कमी पूरा कर लेता। बच्चों को सामान्यतः ईश्वर का प्रतिरूप और देश का भाग्यविधाता कहा जाता है, मगर उन्हीं बच्चों के कोमल हाथों में कुदाल, फावड़ा और सिर पर भारी बोझ तथा आँखों में निरन्तर आँसू बहते देख कर भी हम प्रायः अनदेखा कर देते हैं। आखिर क्या कारण है और उसका क्या निराकरण है। |
||||||
| अध्ययन का उद्देश्य | इस लेख का मुख्य उद्देश्य यह है कि बाल श्रमिकों की स्थिति, चुनौतियां और समाधान विषयक विधियों, नियमों का विश्लेषण एवं न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय का परीक्षण करना और इससे संबंधित उत्पन्न चुनौतियों या समस्याओं के निदान पर ध्यान आकृष्ट कराते हु |
||||||
| साहित्यावलोकन | आधुनिक एवं सभ्य कहे जाने वाले समाज में बालश्रम माथे पर एक कलंक की तरह है।
किसी देश की अर्थव्यवस्था उसकी समृद्धि का प्रतीक होता है। वहाँ का हँसता-खेलता, फलता-फूलता बचपन,
इन्हीं बच्चों के सहारे देश का भविष्य टिका होता है और इन्हीं पर देश की
खुशहाली और विकास निर्भर करता है। किन्तु इन बच्चों में बड़ी संख्या उन बच्चों की
भी होती है जिनका बचपन संघर्षों में ही बीता है। मनुष्य जब एक नन्हे शिशु के रूप में जन्म लेता है तो उसे यह नहीं पता होता कि
उसने राजा के घर में पहली बार रूदन किया या रंक के घर में उसे तो यह तब पता चलता है
जब वह अपने जिन्दगी के दो चार वर्ष इस विषम समाज में गुजार देता है। उसे तो तब
मालूम होता है जब उसकी माँ उसकी भूख शांत कराने के लिए उसे दूध तक नहीं पिला पाती, क्योंकि न तो उसके पास इतने पैसे होते हैं ना तो वह स्तनपान
कराने में सक्षम होती है क्योंकि वह तो खुद पहले से कुपोषित है और कुपोषण के कारण
उसके स्तन कब से सूख चुके होते हैं,
और यहीं से शुरू होता है उसके दुर्भाग्य का खेल। प्राचीन इतिहास में, प्राचीन काल से वर्तमान समय
तक बालश्रम का प्रचलन रहा है। पश्चात् समाज में भी बलश्रम का प्रचलन था और बालकों
का सस्ते दास के रूप में शोषण किया जाता था।[1]
भारत में आज करोड़ों बच्चे न्यूनतम पारिश्रमिक दर पर दिन रात मजदूरी करने को
मजबूर हैं। फलस्वरूप उनका बचपन एवं भविष्य अंधकारमय है। स्वतंन्त्रता के बाद हमारे
देश में आज भी हमारा समाज बालकों का शोषण करता चला आ रहा है। लोग कहते हैं कि किसी
समस्या का समाधान शिक्षा है परन्तु यह सांत्वना मात्र है। जब हम किसी का बचपन लौटा
नहीं सकते तो हमें छीनने का भी हक नहीं है।[2] उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पी0एन0 भगवती तथा न्यायमूर्ति रंगनाथ
मिश्र ने यह विचार व्यक्त किया कि,
राज्य का यह कर्तव्य बनता है कि वह अपने राज्य के सर्वांगीण विकास को
सुनिश्चित करने की दिशा में भावी कदम उठाये। मानव संसाधन विकास की योजनाओं में हम
बाल विकास को प्राथमिकता दे ताकि हमारा बालक एक सुदृढ़़ नागरिक बन सके जो शारीरिक
दृष्टि से ह्रष्ट-पुष्ट हो, मानसिक रूप से जागरूप तथा
नैतिक दृष्टि से स्वस्थ हो।[3] पुनः न्यायमूर्ति पी0एन0 भगवती तथा आर0एस0 पाठक ने यह विचार व्यक्त किया कि आज
के बालक कल के नागरिक है, उन्हीं के कंधों पर कल के
भारत का भार है, उन्हीं पर राष्ट्र की गरिमा और
विकास निर्भर है।[4] एम0सी0 मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य[5] वाद में मेसिजेन कोल कि कविता को
न्यायमूर्ति हंसरिया ने निर्णित किया है। कविता का अर्थ ये है कि ‘बालक मनुष्य का पिता है’
अर्थात् आज का बालक कल का पिता है। एक साहसी और योग्य पिता बनने की योग्यता
रखने के लिए एक बच्चे का जीवन के विकास काल में अच्छी तरह से देखभाल करना चाहिए। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बालश्रम शिक्षा बोर्ड की स्थापना कर
बालश्रम उन्मूलन हेतु एक स्वतंत्र विभाग स्थापित किया गया है। वर्तमान में विभिन्न
प्रतिबंधों के अतिरिक्त तमाम सरकारी तथा निजी संस्थान बालश्रम उन्मूलन हेतु
क्रियाशील है। बालक किसी भी राष्ट्र या समाज की महत्वपूर्ण सम्पत्ति होती है। अतः उनकी
समुचित सुरक्षा, लालन-पालन, शिक्षा-दीक्षा व पर्याप्त विकास का उत्तरदायित्व भी राष्ट्र
या समाज का होता है क्योंकि कालांतर में यही बच्चे राष्ट्र के उत्थान और निर्माण
के आधार स्तम्भ बनते हैं। नंदन रेड्डी ने लिखा है कि, नियोजन में बालश्रमिकों को
अपना बचपन खो देना पड़ता है। वे शारीरिक व मानसिक विकास, स्वतंत्रता,
मनोरंजन, पौष्टिक आहार आदि सुविधाओं
से वंचित रह जाते हैं। इस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए भारत देश का प्रयास निरन्तर बना हुआ है।
वैधानिक प्रावधानों के तहत बालश्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम जो कि
गुरूपादस्वामी समिति के सिफारिशो के आधार पर लागू किया गया। अधिनियम कुछ निर्दिष्ट
खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है और
अन्य स्थलों पर कामकाजी परिस्थितियों को नियंत्रित करता हे। अधिनियम के तहत गठित
बालश्रम तकनीकी सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर खतरनाक व्यवसायों और
प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। भारत में बालश्रम कानून 1986 पारित हुए लगभग 38
वर्ष हो गए लेकिन जिधर भी नजर जाती है बालश्रम से जूझते हुए बच्चों की फौज नजर आती
है। इस कानून के अतिरिक्त भारत सरकार ने कारखाना अधिनियम, 1948 पारित किया। इस कानून के तहत 14 वर्ष से कम आयु के
बच्चों के नियोजन को निषिद्ध करता है और 15-18 वर्ष तक के किशोर किसी कारखाने में
तभी नियुक्त किये जा सकते हैं जब उनके पास अधिकृत चिकित्सक का प्रमाण-पत्र हो।[6] समेकित बाल संरक्षण योजना, महिला एवं बाल विकास
मंत्रालय, भारत सरकार की एक विस्तृत
योजना है। जिसका उद्देश्य देश में बच्चों के लिए एक संरक्षणकारी वातावरण तैयार
करना है।[7] वर्ष 1980 में कैलाश सत्यार्थी ने बचपन बचाओ आन्दोलन की शुरूआत की जिसके द्वारा
अब तक लगभग 01 लाख बच्चों के जीवन को तबाह होने से बचा चुके है। इसी क्रम मे खदान
आधि0 1952, निःशुल्क और अनिवार्य बाल
शिक्षा का अधिकार 2004, बाल संरक्षण आयोग 2007, बालश्रम संशोधन विधेयक 2016 आदि वैधानिक कानूनों के द्वारा
बालश्रम जैसी कुप्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। विधियां- भारतीय संविधान में बालश्रम को रोकने के लिए संवैधानिक प्रावधानो की
महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारतीय संविधान के भाग-3 मूल अधिकार से सम्बन्धित है।
इस भाग के तहत अनु0-23 और अनु0-24 के तहत बालश्रम को निषिद्ध करता है। अनु0-23 बलातश्रम
पर प्रतिबंध लगाता है तथा अनु0-24,
14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी कारखाने या खान में कार्य करने के
लिए नियोजित और न ही किसी अन्य खतरनाक नियोजन में नियुक्त किया जायेगा। अनु0-15(3)
भी यह उपबंधित करता है कि बालकों के लिए विशेष उपबंध बनाने से रोका नहीं जा सकता।
अनु0-21(क) 06 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद-39 (ड.) बालकों की सुकुमार अवस्था को दुरूपयोग न
हो और अनु0-39 (च) बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के
अवसर और सुविधाएँ दी जाये और बालकों और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और
आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। अनुच्छेद-45 राज्य 06 वर्ष की आयु के सभी बच्चों
के पूर्व बाल्याकाल की देख-रेख और शिक्षा देने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 51(क), (ट) 06 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के माता- पिता
उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। इन सबके बावजूद भी बालश्रम जैसी कुप्रथा चली आ
रही है साथ ही उपरोक्त कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है। मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य[8] के बाद में उच्चतम
न्यायालय ने निर्णित किया कि शिक्षा पाने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक
नागरिक का मूल अधिकार है। जिसे उच्चतम न्यायालय ने यूनीकृष्णन बनाम आन्ध्र
प्रदेश [9] के बाद में भी पुष्टि कर दी। सुजीत राय बनाम राजस्थान राज्य[10] के वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णीत किया कि
न्यूनतम मजदूरी अधि0 के तहत निर्धारित मजदूरी से कम भुगतान करना बलातश्रम या बेगार
है जो न्यायोचित नहीं है। बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ[11] के वाद में उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय एवं
राज्य सरकारों को निर्दिष्ट किया कि महिलाओं एवं बच्चों को न्यूनतम मजदूरी का
भुगतान सुनिश्चित किया जाये। अन्तर्राष्ट्रीय परिपेक्ष्य में देखा जाय तो बच्चों के कल्याण और सुरक्षा के
प्रति लगाव कोई नया नहीं है। यह पिछले 70-80 वर्षों से रही है। किन्तु पिछले करीब
4 दशकों से इसने अपनी गति पकड़ ली है। अतः बच्चों के अधिकार का अन्तर्राष्ट्रीय
स्तर पर विकास भी तीव्र गति से हुआ है। सम्भवतः अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के
विकास अधिकार के संरक्षण का विकास 1924 में राष्ट्र संघ के तत्वावधान में प्रारम्भ
होता है। जब बच्चों के अधिकार के जेनेवा घोषणा पत्र अंगीकार किया गया। इसके
पश्चात् मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा,
जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 10 दिसम्बर 1948 को अंगीकार किया ने
बच्चों के अधिकार के संरक्षण के लिए कतिपय उपाय अंगीभूत किये।[12] 1959 में एक बड़ी
महत्वपूर्ण घटना घटी जब संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 20 नवम्बर को बच्चों के
अधिकार की इस घोषणा को अग्रसर करने और इस क्षेत्र में कुछ नया करने के लिए संयुक्त
राष्ट्र की महासभा ने वर्ष 1979 को ‘बाल अधिकारों को
अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष’ घोषित किया।[13] बच्चों के अधिकार को संरक्षण और गारण्टी देने
वाले आज 05 अन्तर्राष्ट्रीय दस्तावेज विद्यमान है। बाल अधिकार पर अन्तर्राष्ट्रीय
स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयासों के अलावा विभिन्न संस्थाओं ने भी इस तरफ
अपना ध्यान केन्द्रित किया है। उनमें से संयुक्त राष्ट्र संघ बाल निधि (युनिसेफ)
प्रमुख है जो बच्चों के अधिकार और कल्याण,
इस संगठन का प्रधान सरोकार है। यह प्रतिवर्ष दुनिया के बच्चें की स्थिति नामक
रिपोर्ट प्रकाशित करता है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसके प्रयत्नों से बच्चों के अधिकार के घोषणा से
प्राप्त होता है। यह संस्था बच्चें के अधिकार और कल्याण की देखभाल करता है।
अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कर्मकारों (जिसमें बच्चे भी आते हैं) संरक्षण प्रदान
करना इसका मुख्य सरोकार है। अपनी स्थापना काल से ही यह संगठन बालश्रम के विरूद्ध
संघर्ष में अग्रणी रहा है और इसके क्रिया-कलापों ने बच्चों के अधिकार के संरक्षण
और बालश्रम में कमी लाने मे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक
संगठन (यूनेस्को), एक अन्य अन्तर्राष्ट्रीय
संस्था जो बच्चों के शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक
आवश्यकताओं की पूर्ति की देखभाल करती है। बाल अधिकारों का अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय
1989 बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए कानूनी और नैतिक आधार प्रस्तुत करता है।[14] अभिसमय में जिन दायित्वों को निभाने का वचन
दिया गया है, समझौते में शामिल देशों
द्वारा उनकी प्राप्ति मे सफलता की जाँच के लिए बाल अधिकार समिति का गठन अनु0-43 के
प्रावधानों के अनुसार किया गया। बाल अधिकारों के अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय के साथ अब
दो प्रोटोकाल भी जुड़े गये है- 1. बालकों के सशस्त्र संघर्ष में शामिल होने से सम्बन्धित ऐच्छिक प्रोटोकाल, जो कि बालको को युद्ध में भर्ती और प्रयोग को सीमित करता
है। 2. बालकों के विक्रय बाल वेश्यावृत्ति और बालकों के अश्लील चित्र से सम्बन्धित
ऐच्छिक प्रोटोकाल, जो कि राज्य सरकारों या
पक्षकारों को यह आदेश देता है कि वे अपने राज्य क्षेत्र में बाल विक्रय, बाल वेश्यावृत्ति और बालकों के अश्लील चित्र पर प्रतिबंध
लगाये।
बच्चों के अधिकार और कल्याण को सुनिश्चित करने लिए न्यूयार्क में शिखर सम्मेलन
1990 आयोजित किया गया। सम्मलेन में 30 सितम्बर 1990 को एक घोषणा जारी किया गया
जिसे बच्चों के उत्तरजीवन, संरक्षण और विकास की विश्व
घोषणा के नाम से जाना गया। |
||||||
| निष्कर्ष |
उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बालश्रम से सम्बन्धित महत्वपूर्ण कदम उठाये गये। इन सबके बावजूद बालश्रम की कुप्रथा निरन्तर बनी हुई है जो कि चिंता तथा समाज के लिए अभिशाप है। वर्तमान में विश्व में सर्वाधिक बालश्रमिक भारत देश में ही है जो कि चिंता का विषय है। बालश्रमिक का स्पष्ट आकड़ा फिलहाल देना कठिन है, परन्तु वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 5-14 वर्ष के 25.96 करोड़ बच्चें में से 1.01 करोड़ बच्चे बालश्रम में लिप्त है जिसकी संख्या वर्तमान में बढ़कर लगभग 05 करोड़ हो गयी है।[15] अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, आज सम्पूर्ण विश्व में करीब 15 करोड़ बच्चे बालश्रम कर रहे हैं।[16] युनिसेफ के अनुसार-दुनियाभर के कुल बाल मजदूरों में 12 फीसदी हिस्सेदारी अकेले भारत की है।[17] सम्पूर्ण विश्व में 05-17 वर्ष के बीच 15.2 करोड़ कामकाजी बच्चे हैं जिसमें 08 करोड़ बच्चे भारत में है। 15.2 करोड़ मिलियन में से 73 लाख बच्चे खतरनाक व्यवसायों/प्रक्रियाओं में काम कर रहे हैं।[18] जो दर्शाता है कि सरकार के प्रयासों ने वांछित परिणाम हासिल नहीं किये है। वर्तमान भारत के भविष्य की नीव जब इतनी मजबूत रखी जा रही है तो फिर ये बालक जिनका इस संसार में आना एक अभिशाप की तरह क्यों मालूम पड़ता है। वर्तमान परिस्थितियों में बालश्रम के लिए जितना कुछ किया जा रहा है सब एक दिखावटी मालूम जान पड़ता है। ये सारी चीजे हाथी के दाँत के हैं। जिसका वास्तविकता से कोई सम्बन्ध नहीं है। बालश्रम सम्बन्धित योजनाएँ अगर वास्तविक रूप में धरातल पर कार्यरत होती तो शायद बच्चों की स्थिति इस प्रकार न होती। बालश्रम की समस्या देश के समक्ष अभी भी एक चुनौती बन कर खड़ी है। सरकार इस समस्या को सुलझाने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है। फिर भी वास्तविक परिणाम हासिल नहीं किया जा सका। समस्या के विस्तार और परिणाम पर विचार किया जाये तो यह पाया जाता है कि यह एक सामाजिक, आर्थिक समस्या के साथ-साथ विकट रूप से गरीबी और निरक्षरता से जुड़ी है। इस समस्या को सुलझाने के लिए समाज के सभी वर्गों को एक साथ आने की जरूरत है। बच्चे राष्ट्र की अमूल्य निधि है तथा इस निधि को सम्पूर्ण सुरक्षा प्रदान करना एवं इनके मनोसामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक मूल्यों के विकास का दायित्व केवल उन परिवारों का ही नहीं है जहाँ ये बच्चे जन्म लेते हैं, वरन् उस समाज तथा देश का भी है जहाँ ये बड़े होते हैं तथा निवास करते हैं। बालश्रम के शोषण की यह परम्परा, जो समाज में एक मानवीय कलंक के रूप में व्याप्त है, उसे तभी समाप्त किया जा सकेगा जब देश का प्रत्येक नागरिक यह सुनिश्चित करे कि बच्चों का बचपन सुरक्षित है कि नहीं। |
||||||
| सन्दर्भ ग्रन्थ सूची | पुस्तके 1. पाण्डेय, डॉ0 जय नारायण, भारत का संविधान (इलाहाबाद सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, 44वॉ संस्करण, 2022) 2. मिश्र, प्रो0 सूर्य नारायण, श्रम एवं औद्योगिक विधि (इलाहाबाद सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, 18वॉ संस्करण, 2012) 3. नरूला एवं तम्बोली, बाल विधियॉ (इलाहाबाद लॉ पब्लिकशन प्रथम संस्करण, 2019 जनवरी 01) 4. अग्रवाल, डॉ0 एच0 ओ0, अन्तराष्ट्रीय विधि एवं मानवाधिकार (इलाहाबाद लॉ पब्लिकेशन 11वॉ संस्करण, 2010) 5. डॉ0 बावेल बसन्ती लाल, महिला एवं बाल कानून (इलाहाबाद सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी 6वॉ संस्करण, 2017) 6. दशोरा मुकेश कुमार, बाल श्रमिक समस्या एवं समाधान(दिल्ली, हिमाशु पब्लिकेशन, प्रथम संस्करण, 2006 कानून- 1. बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधि0 1986 2. कारखाना अधि0 1948 3. खदान अधि0 1952 4. निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2004 5. बाल श्रम संशोधन विधेयक 2016 समाचार पत्र- 1. जनसत्ता 2. ए0वी0पी0 न्यूज 3. आजतक न्यूज पत्रिकाएं- 1. इंडिया टूडे 2. क्रानिकल वेवसाइट- 1. www. Aajtak.intoday.in 2. www.Abplive.com>india 3. www.abplive.com>india महत्वपूर्ण मामले- 1. लेबर एण्ड इन्ट्रीयल केसेज 1998 पेज सं0-567 2. शीला वर्से बनाम भारत संघ चिल्ड्रन एण्ड सोसायटी AIR 656 3. शीला वर्से बनाम भारत संघ AIR 1986 SC, Page-197 4. एम0सी0 मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य (1996)6 SCC 5. मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य (1992) 3 SCC 666 6. यूनीकृष्णन बनाम आन्ध्र प्रदेश (1993) 4 SCC 645 7. सुजीत राय बनाम राजस्थान राज्य (1983) 1SCC 525 8. बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ AIR 1984 SC802 |
||||||
| अंत टिप्पणी | 1. योजना, नवम्बर 2020, पृष्ठ संख्या-17 2. कुलश्रेष्ठ जे0सि0 चाइल्ड लेबर इन इण्डिया (2001), पेज सं0-7 3. शीला वर्से बनाम भारत संघ AIR 1986 SC, Page-197 4. शीला वर्से बनाम भारत संघ चिल्ड्रन एण्ड सोसायटी AIR 656 5. लेबर एण्ड इन्ट्रीयल केसेज 1998 पेज सं0-567 6. एम0सी0 मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य (1996)6 SCC 7. NDTV.com Articles 8. (1992) 3 SCC 666 9. (1993) 4 SCC 645 10. (1983) 1SCC 525 11. AIR 1984 SC802 12. भारत की बाल नीति (14 अगस्त 1974), संख्या-1, पुष्ठ-74 13. 21 दिसम्बर 1976 को पारित संकल्प पत्र के माध्यम से। 14. अनुच्छेद 17(5) 15. Aajtak.intoday.in 16. Abplive.com>india 17. Abplive.com>india 18. abplive.com>india |
||||||